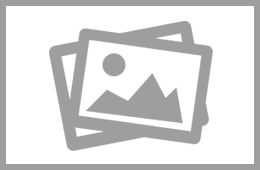संस्कारों का कब्रिस्तान बॉलीवुड
हमारा देश अपनी गौरवमयी संस्कृति के लिए ही विश्व भर में गौरवान्वित रहा है परंतु हम पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में अपनी संस्कृति भुला बैठे और सुसंस्कृत कहलाने की बजाय सभ्य कहलाना अधिक पसंद करने लगे। जिस देश में धन से पहले संस्कारों को सम्मान दिया जाता था, वहीं आजकल अधिकतर लोगों के लिए धन ही सर्वेसर्वा है। धन-संपत्ति से ही आजकल व्यक्ति की पहचान होती है न कि संस्कारों से। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है...
*वित्तमेव कलौ नॄणां जन्माचारगुणोदयः ।
धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि॥*
अर्थात् "कलियुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा, वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा।"
आजकल यही सब तो देखने को मिल रहा है, जो ज्ञानी हैं, संस्कारी हैं, गुणी हैं किन्तु धनवान नहीं हैं, उनके गुणों का समाज में कोई महत्व नहीं, लोगों की नजरों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है न ही उनके कथनों का कोई मोल परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कहे जो समाज में धनाढ्यों की श्रेणी में आता हो तो उसकी कही छोटी से छोटी बात न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि अनर्गल होते हुए भी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है और यही कारण है कि निम्नता की सीमा पार करके कमाए गए पैसे से भी ये बॉलीवुड के कलाकार प्रतिष्ठित सितारे कहलाते हैं। आज भी हमारी संस्कृति में स्त्रियाँ अपने पिता, भाई और पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के गले भी नहीं लगतीं (ये गले लगने की परंपरा भी बॉलीवुड की ही देन है) न ही ऐसे वस्त्र धारण करती है जो अधिक छोटे हों या स्त्री के संस्कारों पर प्रश्नचिह्न लगाते हों, परंतु हमारे इसी समाज का एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पुरुष व स्त्रियाँ खुलेआम वो सारे कृत्य करते हैं जिससे न सिर्फ स्त्रियों के चरित्र पर प्रश्नचिह्न लगता है बल्कि समाज में नैतिकता का स्तर भी गिरता है।
आजादी के नाम पर निर्वस्त्रता की मशाल यहीं से जलती है और समाज में बची-खुची आँखों की शर्म को भी जलाकर राख कर देती है और शर्मोहया की चिता की वही राख बॉलीवुड की आँखों का काजल बनती है।
पैसे कमाने के लिए ये मनोरंजन और कला के नाम पर समाज में अश्लीलता और अनैतिकता परोसते हैं और आम जनता मुख्यत: युवा पीढ़ी इनकी चकाचौंध में फँसकर धीरे-धीरे अंजाने ही वो सब करने लगती है जिससे समाज में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है।
महात्मा गाँधी ने अपनी जीवनी में लिखा था कि उन्होंने एक बार बाइस्कोप में राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखी और उसका उनके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने उसी समय से हमेशा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की। अब प्रश्न उठता है कि यदि चित्र के रूप में देखी गई कोई कहानी एक बार में किसी किशोर हृदय पर इतना असर छोड़ सकती है, तो वर्तमान समय में जब बच्चे, किशोर और युवा चलचित्र के रूप में अश्लीलता को रोज-रोज देखते हैं तब उनके हृदय पर कितना असर पड़ता होगा!!! यह समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए काफी है।
एक समय था जब हमारे ही देश में पहली हिन्दी फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' में हिरोइन के लिए कोई महिला नहीं मिली तो पुरुष ने महिला का रोल निभाया था और आज का समय है कि जितने कम वस्त्र उतने अधिक पैसे वाली थ्योरी पर चल रहे बॉलीवुड में थोड़े से पैसे और नाम के लिए अभिनेत्रियाँ कम से कम वस्त्रों में फोटो खिंचवाती हैं। वही बॉलीवुड कलाकार युवा पीढ़ी के आदर्श बन जाते हैं जिनका स्वयं का कोई आदर्श, कोई उसूल नहीं या फिर ये कहें कि उनके आदर्श और उसूल बस पैसा ही है परंतु विडंबना यह है कि जनता और सरकार सभी इनकी सुनते हैं।
ये मनोरंजन के नाम पर नग्नता और व्यभिचार दर्शा कर जहाँ एक ओर समाज के युवा पीढ़ी को बरगलाते हैं वहीं आजकल टीवी, सिनेमा, मोबाइल, लैपटॉप जैसे आधुनिक तकनीक छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में किताबों की जगह ले चुके हैं, फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया से कोई कब तक अछूता रह सकता है। चाहकर भी बच्चों को इनसे दूर नहीं रखा जा सकता और इनमें संस्कार और नैतिकता के पाठ नहीं पढ़ाए जाते बल्कि स्त्रियों की आजादी के नाम पर अंग प्रदर्शन, युवाओं की आजादी के नाम पर खुलेआम अश्लीलता फैलाना, ये सब आम बात हो चुकी है। इतना ही नहीं वामपंथी विचारधारा के समर्थक और प्रचारक बॉलीवुड में भरे पड़े हैं और ये समाज में होने वाले सभी प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करके उन्हें मजबूती देते हैं।
मेहनत तो एक आम नागरिक भी करता है और अपनी मेहनत से कमाए गए उन थोड़े से पैसों से ही अपना परिवार पालता है परंतु अधिक पैसों के लालच में अपने संस्कार नहीं छोड़ता अपनी लज्जा को नहीं छोड़ता परंतु उस सम्मानित किंतु साधारण व्यक्ति की बातों का कोई महत्व नहीं वह कुछ भी कहे किसी को सुनाई नहीं देता लेकिन यही अनैतिक और संस्कार हीन सेलिब्रिटी यदि छींक भी दें तो अखबारों की सुर्खियाँ और न्यूज चैनल के ब्रेकिंग न्यूज बन जाते हैं, इसीलिए तो इनका साहस इतना बढ़ जाता है कि ये ग़लत चीजों या घटनाओं का खुलकर समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि सरकार उनकी अनर्गल बातों का आदेशों की भाँति पालन करे। बॉलीवुड से राजनीति में आना तो आजकल चुटकी बजाने जितना आसान हो गया है क्योंकि सब पैसों और प्रसिद्धि का ही खेल है। जिसके पास बॉलीवुड और राजनीतिक कुर्सी दोनों का बल होता है, वो अपने आप को ही राज्य या देश मान बैठे हैं, इसीलिए तो बिना सोचे समझे ही निर्णय सुना देते हैं कि जिसने हमारे विरुद्ध कुछ कहा उसने अमुक राज्य का अपमान किया और उसे अमुक राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। किसी को लगता है कि महाराष्ट्र के बाहर से आए बॉलीवुड में काम करने वाले सभी सितारे उनकी दी हुई थाली (बॉलीवुड) में खाते हैं अर्थात् बॉलीवुड रूपी थाली उन्होंने ही दिया था, दिन-रात जी-तोड़ परिश्रम का कोई महत्व नहीं, इसलिए यदि ये दिन को रात और रात को दिन या ड्रग्स को टॉनिक कहें तो उस बाहरी सितारे को भी ऐसा ही करना चाहिए, नहीं किया तो किसी का घर तोड़ दिया जाएगा या किसी की हत्या कर दी जाएगी।
देश के किसी भी कोने में देश के हित में लिए गए किसी निर्णय का विरोध करना हो या हिन्दुत्व विरोधी प्रदर्शन करना हो या सरकार को अस्थिर करने के लिए किसी असामाजिक कार्य का समर्थन करना हो तो ये जाने-माने सितारे हाथों में तख्तियाँ लेकर फोटो खिंचवा कर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं किंतु जब कहीं सचमुच अन्याय हो रहा हो या कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो तब ये तथाकथित प्रतिष्ठित लोग कहीं नजर नहीं आते।
समाज में नैतिकता के गिरते स्तर का जिम्मेदार बॉलीवुड ही है और उदाहरणार्थ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जाँच के दौरान नशालोक की सच्चाई सामने आने लगी और बॉलीवुड के नशा गैंग की संख्या द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती ही जा रही है। जहाँ बाप-बेटी के रिश्ते की मर्यादा नहीं होती, जहाँ दिन-रात गांजा ड्रग्स के धुएँ के बादल घिरे रहते हैं, जहाँ इन वाहियात कुकृत्यों का समर्थन न करने वालों के लिए मौत को गले लगाने के अलावा कोई स्थान नहीं...हम उसी बॉलीवुड की फिल्मों को देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं और इनकी अनैतिकता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये बॉलीवुड हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों का कब्रिस्तान है। इसकी शुद्धि जनता के ही हाथ में है नहीं तो कहते हैं न कि 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता।' यदि जनता एक साथ इन्हें सबक नहीं सिखाती तो अकेले आवाज उठाने वाला कब कहाँ अदृश्य हो जाए कुछ पता नहीं होता, या फिर उसका घेराव करके उसकी आवाज को ही नकारात्मक सिद्ध कर दिया जाता है।
जनता मुख्यत: आज की युवा पीढ़ी को इन्हें बताना होगा कि उन्हें आदर्शविहीन अनैतिक सामग्री से भरी फिल्में स्वीकार नहीं और न ही ऐसी अश्लीलता परोसने वाले फिल्मी सितारों को अपना आदर्श मान सकते हैं। देश को अनैतिक संस्कारहीन सेलिब्रिटी की नहीं बल्कि ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो हमारे देश की संस्कृति के रक्षक बन सके न कि उसे विकृत करके इसकी छवि को धूमिल करें।
चित्र- साभार गूगल से
मालती मिश्रा 'मयंती'✍️
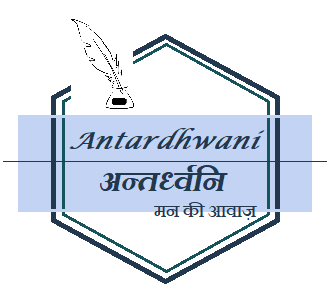




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)